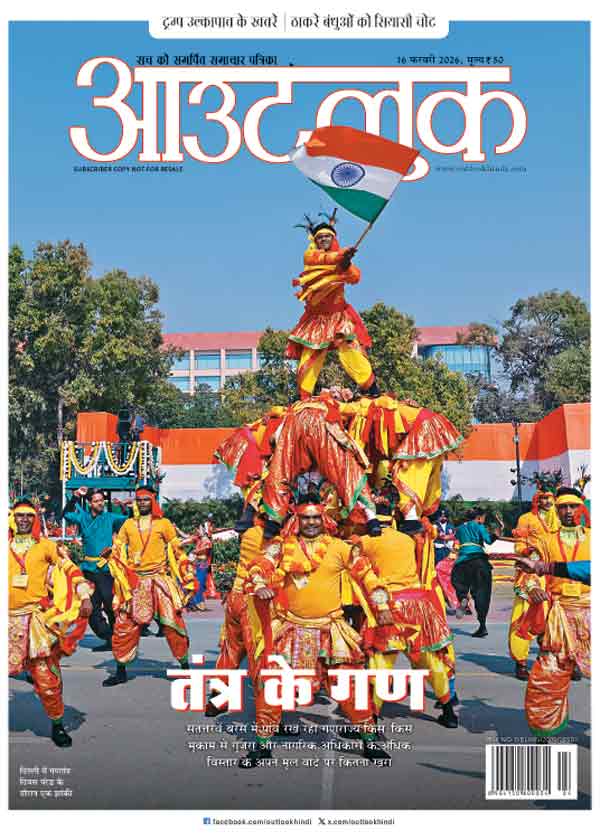कैसी उल्टी गंगा बह रही है! एक जमाने में भारत पूरी दुनिया को महात्मा गांधी का संदेश दिया करता था और अब विदेशों से महात्मा गांधी का संदेश भारत को दिया जा रहा है। एक समय पूरी तीसरी दुनिया में भारत लोकतंत्र की मशाल के रूप में जाना जाता था, आज हालत यह है कि उसे लोकतंत्र के बारे में दूसरे देशों के उपदेश सुनने पड़ रहे हैं। कारण स्पष्ट है। पिछले वर्षों में उसने गांधी और लोकतंत्र, दोनों की उपेक्षा की है। क्योंकि यह सब सरकार और सत्तारूढ़ दल और उसके समानधर्मा एवं सहमना संगठनों के संरक्षण में हुआ है, इसलिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा गांधी के महत्व एवं लोकतंत्र की रक्षा की आवश्यकता पर कुछ बातें सुननी पड़ीं।
महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाने का अर्थ उनके जीवन के मर्म को समझना है। उन्होंने एक बार कहा था कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। सत्य उनके जीवन का केंद्रीय मूल्य था और इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को “सत्य के प्रयोग” का नाम दिया था। सत्य का अर्थ केवल झूठ न बोलना नहीं है। इसका अर्थ किसी भी स्थिति के सार को समझ कर आचरण करना है। सत्य से ही अहिंसा, सभी धर्मों और समुदायों के प्रति समभाव, सहिष्णुता, अच्छाई के प्रति निष्ठा और राग-द्वेष से दूर रहने की शक्ति जैसे गुण नि:स्रत होते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि अहिंसा को केवल शक्तिशाली ही अपने जीवन और आचरण में उतार सकता है, कमजोर नहीं। लेकिन आज हम एक ऐसे समय और समाज में रह रहे हैं जिसे “पोस्ट-ट्रूथ” अर्थात् “उत्तर-सत्य” कहा जाता है।
विभिन्न विचारकों ने इसे विभिन्न तरीक़ों से व्याख्यायित किया है लेकिन सबसे अधिक प्रचलित व्याख्या यह है कि “उत्तर-सत्य” समाज में किसी मुद्दे पर जनता की राय के बनने की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ तथ्यों की भूमिका बेहद कम और भावनाओं एवं निजी विश्वासों की भूमिका निर्णायक होती है। विवेकशीलता का पतन एवं क्षरण, सार्वजनिक विमर्श के क्षेत्र का संकुचन, झूठी या गुमराह करने वाली सूचनाओं का प्रसार, झूठी खबरें, सांस्कृतिक संघर्ष, लोकप्रियता को वैधता में बदलना, सामाजिक मीडिया और तकनीकी का इस्तेमाल किसी विचारधारा विशेष के प्रचार और किसी अन्य के विरोध में इस्तेमाल करना—उत्तर-सत्य समाज के अनेक लक्षणों में से ये कुछेक लक्षण हैं। 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के पहले और बाद में अब तक उनके ख़िलाफ़ दुष्प्रचार नए-नए रूप धारण करता रहा है।
महात्मा गांधी हों या कोई और राजनेता, लेखक, विचारक या कलाकार, कोई भी आलोचना से परे नहीं है। हरेक के विचारों और कामों की वैकल्पिक वैचारिक आधार पर आलोचना की जा सकती है। लेकिन वह आलोचना उस व्यक्ति के विचारों को अच्छी तरह समझे बिना नहीं हो सकती। किसी भी बौद्धिक विमर्श की यह पहली शर्त है कि उसमें आलोच्य विषय का प्रामाणिक प्रतिपादन करने के बाद ही उसकी आलोचना के लिए प्रवृत्त हुआ जाए। ऐसा हुआ भी है। मसलन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से करके अंततः कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर देश के शीर्षस्थ नेताओं में गिने जाने वाले ई एम एस नम्बूदिरिपाद ने ‘महात्मा और उनका वाद’ नामक पुस्तक लिख कर अपनी आलोचना प्रस्तुत की थी। लेकिन पिछले आठ दशकों के दौरान महात्मा गांधी के बारे में नितांत झूठी बातें लिखकर उनके आधार पर आलोचना करने का काम भी होता रहा है। जबसे इंटरनेट आया है, तबसे इस काम में असाधारण रूप से तेज़ी आयी है और अनेक वेबसाइटें महात्मा गांधी की फ़ोटोशॉप के ज़रिए फ़र्ज़ी तस्वीरें बनाकर उन्हें प्रचारित-प्रसारित करती रहती हैं। इसी तरह से उनके जीवन के बारे में नितांत झूठी और कुत्सित सूचनाएँ भी प्रसारित की जाती रहती हैं। उनकी हत्या का औचित्य सिद्ध करने के प्रयास में भी तेज़ी आयी है। भारत-विभाजन के लिए भी उन्हें और जवाहरलाल नेहरु को ही प्राथमिक रूप से दोषी ठहराया जाता है। इनके बरक्स सरदार पटेल को खड़ा करके यह भी कहा जाता है कि यदि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो न कश्मीर समस्या पैदा होती और न ही मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनायी जाती। इन क्रम में पटेल को नेहरु के विरोध में खड़ा करके दोनों की तुलना की जाती है। नेहरु भी गांधी की तरह दुष्प्रचार का शिकार रहे हैं और हैं। गांधी का जीवन साम्प्रदायिक सद्भाव को समर्पित था। उनके जीवन के अंतिम वर्ष तो इस मामले में पूरे विश्व के सामने मिसाल प्रस्तुत करते हैं। यह अकारण नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके बारे में लिखा था कि आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास नहीं कर पाएंगी कि कभी उनके जैसा हाड़-माँस का बना जीता-जागता आदमी भी इस पृथ्वी नामक ग्रह पर चलता-फिरता था। उनसे प्रेरणा ग्रहण करने वालों में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे संघर्षशील योद्धा तो शामिल थे ही, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी अक्सर उनका उल्लेख करते थे।
हत्या के एक दिन पहले 29 जनवरी, 1948 को प्रार्थना सभा में बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहा था: “मेरी चले तो हमारा गवर्नर-जनरल किसान होगा, हमारा बड़ा वज़ीर किसान होगा, सब कुछ किसान होगा, क्योंकि यहाँ का राजा किसान है।….किसान ज़मीन से पैदा न करे तो हम क्या खाएँगे? हिंदुस्तान का सचमुच राजा तो वही है।” वही किसान पिछले एक साल से सड़क पर है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और टिप्पणीकार हैं। यहां व्यक्त विचार निजी हैं)