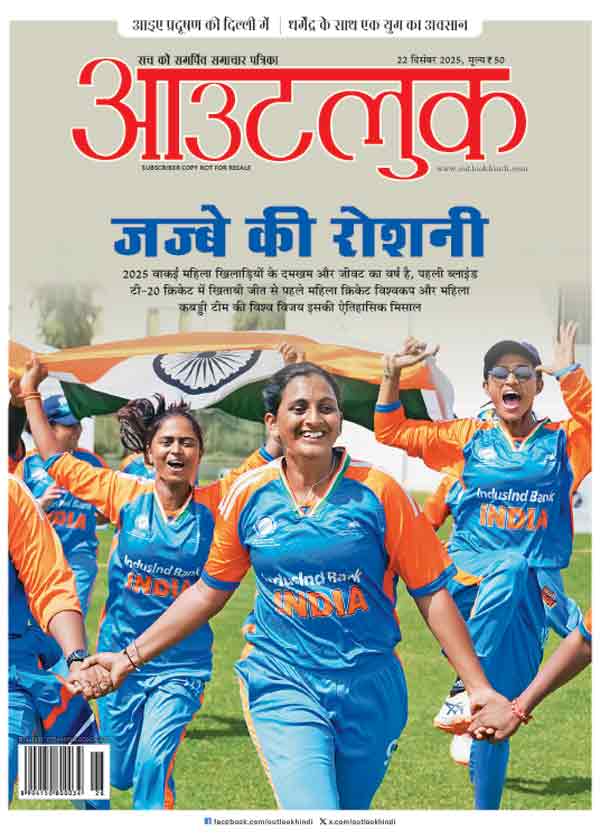भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ भाषा और राजनीतिक मुद्दे अक्सर परस्पर जुड़े होते हैं। हाल के दिनों में तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, त्रिभाषा फॉर्मूला, हिंदी विरोध और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर बड़े विवाद उभरे हैं। तमिलनाडु में यह संघर्ष केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार और कई क्षेत्रीय दल इसे केंद्र सरकार की नीतियों से उपजा असंतोष मानते हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर सकता है। यह विवाद समय के साथ और गहराता जा रहा है और आने वाले वर्षों में इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।
भारत सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति (एनईपी) लागू की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। इस नीति के तहत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव त्रिभाषा फॉर्मूला है, जिसमें छात्रों को तीन भाषाएँ सीखनी होंगी: मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा, और अंग्रेज़ी या कोई अन्य विदेशी भाषा। तमिलनाडु ने इस नीति का कड़ा विरोध किया, क्योंकि वहाँ पहले से ही “द्विभाषा नीति” लागू है, जिसमें छात्र केवल तमिल और अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार और डीएमके ने इसे “हिंदी थोपने का प्रयास” करार दिया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे तमिल भाषा और संस्कृति के लिए खतरा बताया है।
तमिलनाडु ही नहीं, अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे केरल और आंध्र प्रदेश ने भी हिंदी को अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है। कर्नाटक में भी भाषा को लेकर संवेदनशीलता है, लेकिन वहाँ हिंदी विरोध उतना तीव्र नहीं है जितना तमिलनाडु में देखा जाता है।
तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास दशकों पुराना है। 1930 के दशक में मद्रास प्रेसीडेंसी में हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश की गई थी, जिसका कड़ा विरोध हुआ। इसके बाद, 1965 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें कई लोगों की जान गई थी। इस आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को यह वादा करना पड़ा कि हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं जाएगा।
आज जब नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने की बात हो रही है, तो तमिलनाडु उसी पुराने संघर्ष को दोहरा रहा है। डीएमके और अन्य द्रविड़ दल इसे “भाषाई उपनिवेशवाद” कह रहे हैं। राज्य में हिंदी विरोधी नारों के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों से हिंदी संकेत हटाने और विरोध प्रदर्शन जैसी घटनाएँ सामने आ रही हैं।
परिसीमन (Delimitation) लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया है, जिसमें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है। परिसीमन के नए प्रस्ताव के अनुसार, उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं, जबकि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं।
तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी रूप से अपनाया है, जिससे वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम है। लेकिन परिसीमन के अनुसार, कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की लोकसभा सीटें घट सकती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। इस कारण दक्षिण भारतीय राज्यों में यह भावना है कि वे जनसंख्या नियंत्रण की सजा भुगत रहे हैं।
हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में स्पष्ट किया कि परिसीमन के कारण तमिलनाडु या किसी अन्य दक्षिण भारतीय राज्य की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी। यह बयान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से घटकर 31 हो सकती हैं।
2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, और यह संभावना है कि त्रिभाषा नीति और परिसीमन चुनावी मुद्दे बनेंगे। तमिल पहचान और हिंदी विरोध का मुद्दा राज्य में पहले से ही बड़ा राजनीतिक विषय रहा है, और आगामी चुनावों में यह और अधिक तीव्र हो सकता है। तमिलनाडु के राजनीतिक दल इन मुद्दों को अपनी रणनीति का हिस्सा बना सकते हैं। कुछ नेताओं ने हाल ही में यह बयान भी दिया है कि तमिल लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि भविष्य में तमिल आबादी की राजनीतिक शक्ति बनी रहे। यह बयान परिसीमन से जुड़ी आशंकाओं को दर्शाता है।
तमिलनाडु में हिंदी विरोध, त्रिभाषा फार्मूला और परिसीमन का मुद्दा केवल भाषाई अस्मिता से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शक्ति संतुलन का भी विषय है। दक्षिण भारतीय राज्यों को लगता है कि उन्हें हिंदी थोपने के प्रयासों और राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इन मुद्दों पर सभी राज्यों के साथ सहमति बनाकर समाधान निकाले, ताकि कोई भी राज्य खुद को अलग-थलग महसूस न करे। यदि यह विवाद अनसुलझा रहा, तो यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।
( यह लेखक के निजी विचार हैं)