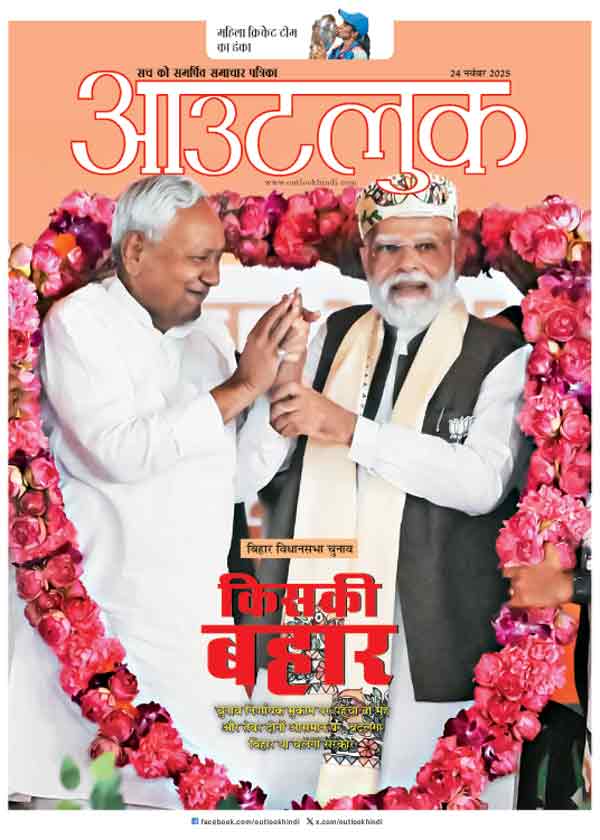एक मुशायरे में दो शायरों ने कलाम पढ़ा तो एक शायर बहुत ज़्यादा पसंद किये गए और दूसरे उनके मुकाबले ज़रा कम रहे, तो उन्होंने ज़्यादा पसंद किये जाने वाले शायर से पूछा कि ‘‘ग़ज़लें तो तुम्हारी और मेरी तकरीबन एक जैसी ही थीं, लेकिन क्या वजह है कि तुम ज़्यादा पसंद किए गए”, तो उन्होंने जवाब दिया कि ‘‘मियाँ, बीवी को देख कर ग़ज़ल कहोगे तो यही हश्र होगा।”
यह बात अपने आप में मज़ाक़ के साथ-साथ शायर का तजुर्बा भी हो सकता है। दरअसल शायरी, साहित्य व कला की किसी विधा को हदों में नहीं बाँधा जा सकता। जिस काव्यगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, यह भी उसका एक पहलू हो सकता है। शायर अपनी सीमाएं खुद तय करता है, तभी उसके कलाम में वह रस और रंग आता है जो उसे सदियों तक ज़िंदा रखता है। यही वजह है कि उर्दू-हिंदी के हज़ारों लिखने वालों में से गिनती के चंद नाम ही मशहूर और अमर हो जाते हैं, यानि अपने फन के लिए अपनेआप को फना करना पड़ता है।
उर्दू शायरी का एक ऐसा ही बांका, अलबेला शायर है ‘‘असरारुल हक़ ‘मजाज़’ लखनवी।” मजाज़ प्रगतिशील शायरों में अपने वक़्त के सब से लोकप्रिय शायर थे। उनकी लोकप्रियता वक़्त के साथ अहमियत में बदलती गयी और मजाज़ उर्दू शायरी का एक ऐसा नाम बन गया जो शायरी के ज़िक्र के दौरान अपनेआप ज़बान पर आ जाता है।
बीसवीं सदी का शुरुआती दौर हिन्दुस्तान के राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक नज़रिए से बहुत अहम् है। शायरी की ही बात करें तो शायरी में भी पुराने अंदाज़ और विषयों को ले कर बेइत्मिनानी थी, नए रुझानों की हवा थी। प्रगतिशील आंदोलन का असर अदब और शायरी पर देखा जा सकता था। मजाज़ उसी दौर की देन हैं।
मजाज़ 11 अक्टूबर 1911 को रुदौली, उत्तरप्रदेश के ज़मींदार घराने में पैदा हुए। उन्हें लाड़-प्यार से पाला गया। उनकी तालीम वहीं शुरू हुई और बाद में उनके वालिद नौकरी के सिलसिले में जब लखनऊ आये तो मजाज़ को भी अपने साथ ले आये। लखनऊ के अमीनाबाद हाईस्कूल से उन्होंने नवीं और दसवीं जमात पास कीं। लखनऊ के शायराना माहौल में ‘असरारुल हक़’ के ‘‘मजाज़’’ बनने का आग़ाज़ हुआ, उनका झुकाव शायरी की तरफ हुआ। फिर वह अपने वालिद के साथ आगरा आ गए और आगरा मजाज़ की ज़िन्दगी का निर्णायक मोड़ साबित हुआ क्योंकि उनका शैरी सफ़र आगरा से ही शुरू हुआ।
मजाज़ आगरा के जिस घर में रहे, उसी के पड़ोस वाले मकान में मशहूर शायर फानी बदायूनी रहते थे। 1921 में मजाज़ का दाखिला सेंट जोन्स कॉलेज, आगरा में कराया गया जहाँ उन्हें भौतिकी और गणित जैसे विषय दिलाए गए, क्योंकि उनके वालिद उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन मजाज़ को तो कुछ और ही बनना था। फिर उनके वालिद का तबादला आगरा से अलीगढ़ हो गया और मजाज़ को पढ़ाई जारी रखने के लिए आगरा में ही छोड़ दिया गया, अब मजाज़ के लिए रास्ते खुले हुए थे। वालिद के अलीगढ़ जाने और मजाज़ के आगरा में तन्हा रह जाने से उनके अन्दर बेचैनी और लापरवाही आ गई, रात-रात भर शायरी की महफिलों में शरीक होने लगे, जिसका असर तालीम पर हुआ लेकिन शायरी में निखार आने लगा।
मजाज़ ने 1921 में पहली ग़ज़ल कही, जो इस तरह है:
हुस्न को बे-हिजाब होना था
शौक़ को कामयाब होना था
तेरे जल्वों में घिर गया आखिर
ज़र्रे को आफ़ताब होना था
कुछ तुम्हारी निगाह काफ़िर थी
कुछ मुझे भी ख़राब होना था...
मजाज़ ने 1931 में कॉलेज के एक मुशायरे में ये ग़ज़ल पढ़ी और उन्हें बेहतरीन ग़ज़ल का स्वर्ण पदक मिला:
यूँ ही बैठे रहो दर्द-ए-दिल से बे-ख़बर हो कर
बनो क्यों चारागर, तुम क्या करोगे चारागर हो कर
ये किसके हुस्न के रंगीन जल्वे छाये जाते हैं
शफ़क़ की सुर्ख़ियाँ बन कर, तजल्ली-ए -सहर हो कर...
घर वाले उन्हें आगरा से अलीगढ़ ले आये और वहां उन्होंने बी.ए. पास किया। अलीगढ़ के इल्मी, अदबी माहौल का उनपर ज़बरदस्त असर हुआ, उनकी सोच को नयी सिम्त मिली और मजाज़ प्रगतिशील आन्दोलन से जुड़े। मजाज़ ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तराना भी लिखा जो आज तक गाया जाता है | अब मजाज़ नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुके थे। उनका घर मीरस रोड पर था जो अलीगढ़ का एक ख़ूबसूरत इलाक़ा था। कहते हैं कि उस सड़क पर लड़कियों का एक कॉलेज था और उस सड़क पर घूमना नौजवानों का पसंदीदा शौक़ था। यूनिवर्सिटी के अन्दर खिलाड़ी, शायर, साहित्यकार, मौलवी, रिंद और जाहिद, पढ़ने-लिखने वाले और बेफिकरे सब मौजूद थे, यानि उन्हें वहां शायरी के लिए बहुत माकूल माहौल मिला और उनकी शायरी उसी माहौल में परवान चढ़ी। वह उस वक़्त के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ही नहीं, चहीते शायर बन गए। उनके एक-एक शेर पर लोग सर धुनते, बार-बार पढ़ने की फरमाईश करते। मजाज़ की ग़ज़लें और नज़्में हर दिल की पुकार बन गयीं और मजाज़ इंतेहाई मक़बूल हो गए। किस्से मशहूर हैं कि लड़कियां उनकी तस्वीरें छुपा कर रखती थीं, उनका कलाम तकिये के नीचे रख कर सोती थीं, उनके नाम की पर्चियां डाली जाती थीं।
अपनी एक नज़्म “तार्रुफ़” में वह अपना तार्रुफ़ इस तरह देते हैं :
खूब पहचान लो असरार हूँ मैं
जिन्स-ए-उल्फ़त का तलबगार हूँ मैं
इश्क़ ही इश्क़ है दुनिया मेरी
फित्नः-ए-अक़्ल से बेज़ार हूँ मैं
कुफ्र-ओ-इलहाद से नफ़रत है मुझे
और मज़हब से भी बेज़ार हूँ मैं
तालीम मुकम्मल करने के बाद मजाज़ एक बरस तक ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली की पत्रिका “आवाज़” के संपादक रहे। इस पत्रिका का नाम “आवाज़” मजाज़ का दिया हुआ है, जो आज भी जारी है। मजाज़ रेडियो में ज़्यादा दिन काम ना कर सके, उसके बाद दिल्ली के हार्डिंग पुस्तकालय में काम किया लेकिन कहीं मुतमईन नहीं हुए। इस बेचैनी और बेइत्मिनानी की कैफियत में शायरी और इश्क़ मजाज़ के लिए राहत का ज़रिया थे मगर वह अपने इश्क़ में नाकाम रहे और उनकी शायरी में निखार आता गया। उस दौर में मजाज़ ने कई ख़ूबसूरत और पुरअसर नज़्में लिखीं जिनमें उन जैसे कई नौजवानों के जज़्बात और तमन्नाओं का अक्स था। नज़्म ‘मजबूरियाँ’ के शेर काबिले-गौर हैं:
मैं आहें भर नहीं सकता, के नग़्मे गा नहीं सकता
सुकूं लेकिन मिरे दिल को, मयस्सर आ नहीं सकता
वो बादल सर पे छाये हैं, कि सर से हट नहीं सकते
मिला है दर्द वो दिल को, कि दिल से जा नहीं सकता
“नौजवान खातून से” वाली जो नज़्म उन्होंने लिखी उसका आख़िरी शेर तो अब मुहावरा बन चुका है:
‘‘तेरे माथे पे ये आँचल बहुत ही खूब है लेकिन,
तू इस आँचल से इक परचम बना लेती तो अच्छा था’’
1937 में उनकी मशहूर नज़्म ‘आवारा’ जब सामने आई तो बेशुमार लोगों के दिल की आवाज़ बन गयी। यह नज़्म देश में उस वक़्त फैली आर्थिक असमानता, जाति संघर्ष और विचारों के टकराव के साथ-साथ मजाज़ जैसे बहुत से नौजवानों की असंतुष्टि का एक सच्चा चित्र है।
पहले और आखिरी बंद काबिले-गौर हैं:
शहर की रात और मैं नाशादो-नाकारा फिरूं
जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं
ग़ैर की बस्ती है, कब तक दर-ब-दर मारा फिरूं
ऐ गमे दिल क्या करूँ ऐ वहशते दिल क्या करूँ
बढ़के इस इन्दर-सभा का साज़ो-सामां फूंक दूं
इसका गुलशन फूंक दूं , उसका शबिस्तां फूंक दूं
तख़्ते-सुल्तां क्या, मैं सारा क़स्रे-सुल्तां फूंक दूं
ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ
मजाज़ की शायरी इंक़लाब और रोमांस का ख़ूबसूरत गुलदस्ता है, हुस्नो-नज़ाकत का दस्तावेज़ भी है। उनकी तीन किताबें प्रकाशित हुईं। ५ दिसंबर, १९५५ को लखनऊ में, ४४ साल की कम उम्र में ही, ये हरदिलअज़ीज़ शायर इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया।
(बद्र वास्ती शायर और लेखक हैं।)