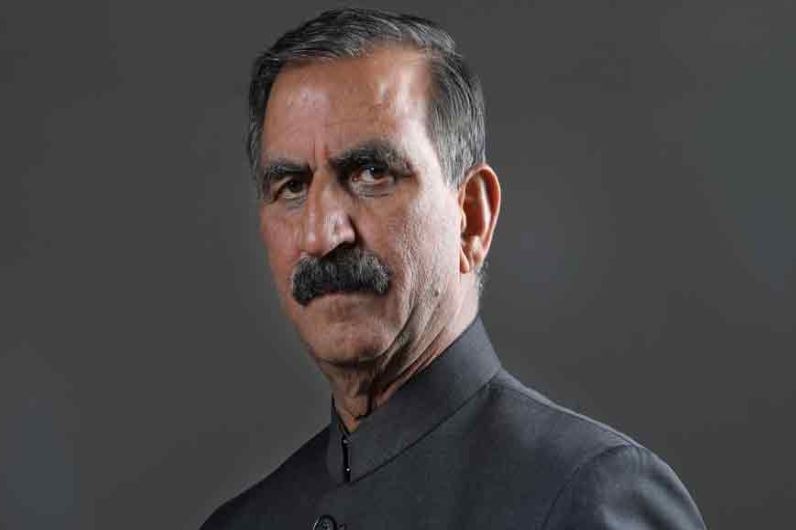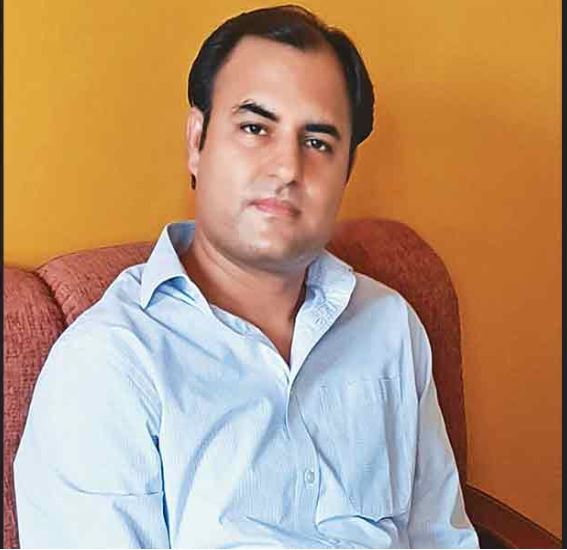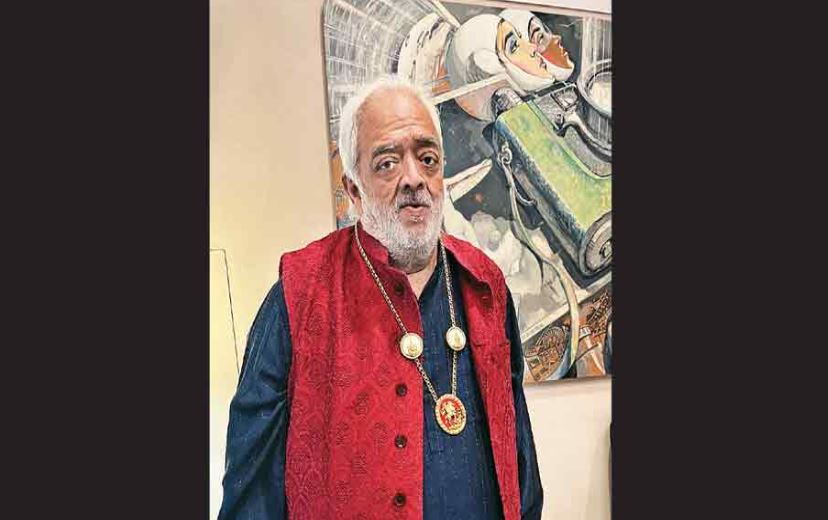भारतीय शहरों में अनियंत्रित ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या आज एक विकराल चुनौती बन चुकी है। बढ़ते शहरीकरण, निजी वाहनों की बढ़ती संख्या और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कमजोरियों ने इस समस्या को और गहरा दिया है। चाहे वह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु हो या लखनऊ और जयपुर, लगभग हर बड़े और मध्यम आकार के शहर में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या आम हो गई है। यह समस्या केवल नागरिकों के समय और ऊर्जा की बर्बादी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी हैं। हर दिन लाखों लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है, ईंधन की खपत बढ़ती है, और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर, पार्किंग की कमी ने सड़कों को अवैध पार्किंग स्थलों में बदल दिया है, जिससे शहरों में अव्यवस्था का माहौल बन गया है।
भारतीय शहरों में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या की जड़ें शहरीकरण और बढ़ते निजी वाहनों में छिपी हैं। 1951 में भारत में केवल 17% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी, जबकि 2021 तक यह आंकड़ा 35% को पार कर गया और 2030 तक इसके 40% तक पहुँचने का अनुमान है। बढ़ती शहरी आबादी के साथ-साथ वाहनों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 50,000 से अधिक नए वाहन पंजीकृत हो रहे हैं। बड़े शहरों में प्रति परिवार औसतन दो वाहनों का स्वामित्व आम हो गया है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की सीमित उपलब्धता और साइकिल या पैदल चलने की संस्कृति का ह्रास भी इस समस्या को और बढ़ा रहा है। लोगों की निजी वाहनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या और विकराल हो रही है।
ट्रैफिक जाम भारतीय शहरों की एक आम समस्या बन गई है। बेंगलुरु, जिसे भारत का ‘आईटी हब’ कहा जाता है, वहां ट्रैफिक की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि औसतन नागरिक हर साल ट्रैफिक में 240 घंटे बर्बाद करता है। TomTom Traffic Index के अनुसार, बेंगलुरु दुनिया के सबसे ट्रैफिक-ग्रस्त शहरों में शामिल हो चुका है। दिल्ली और मुंबई में ट्रैफिक जाम के कारण औसत यात्रा समय 50% से अधिक बढ़ गया है, जिससे नागरिकों का न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि उनकी मानसिक शांति भी भंग होती है। वहीं, पार्किंग की समस्या भी कम भयावह नहीं है। अधिकांश भारतीय शहरों में सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग आम हो गई है, जिससे ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न होती है। शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और ऑफिस कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क किनारे अवैध पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। रिहायशी इलाकों में भी पार्किंग का संकट गंभीर रूप ले चुका है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लोग मजबूरन सड़कों पर पार्किंग करते हैं, जिससे सड़कों की चौड़ाई घट जाती है और ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है।
ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ट्रैफिक में फंसे वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। दिल्ली, मुंबई और कानपुर जैसे शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है। ट्रैफिक जाम में फंसे वाहन अधिक ईंधन जलाते हैं, जिससे CO₂ और अन्य जहरीली गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। ध्वनि प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है, जो नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ट्रैफिक जाम में फंसे लोग मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और अवसाद का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा, यह समस्या आर्थिक नुकसान का भी कारण बन रही है। ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के कारण लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं में देरी होती है, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ता है।
भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वे अब तक पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों को चुना, जहाँ ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का समाधान करने के लिए स्मार्ट तकनीकों का उपयोग किया जाना था। हालांकि, इन योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो पाया। मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विस्तार भी किया गया, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी के कारण लोग अभी भी निजी वाहनों पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP) और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी लागू किया गया, लेकिन यह योजनाएँ ज़मीनी स्तर पर प्रभावी साबित नहीं हो पाईं। कई शहरों में मल्टी-लेवल पार्किंग और स्मार्ट पार्किंग सिस्टम की शुरुआत की गई, लेकिन अवैध पार्किंग पर नियंत्रण न होने के कारण समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।
अगर हम अन्य देशों की बात करें तो कई देशों ने इस समस्या का सफलतापूर्वक समाधान किया है। सिंगापुर में कंजेशन प्राइसिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत ट्रैफिक-जाम वाले इलाकों में प्रवेश करने वाले वाहनों से अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। इससे ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है और लोग सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने लगे हैं। लंदन ने कंजेशन चार्ज और लो-एमिशन जोन की नीति अपनाई है, जिससे ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद मिली है। जापान ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना प्रभावी बनाया है कि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम करते हैं। वहां मेट्रो और ट्रेन नेटवर्क इतना सुलभ और सुविधाजनक है कि लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करते। नीदरलैंड ने साइकिल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम हुआ और प्रदूषण भी घटा।
भारत में भी इन सफल उदाहरणों से सीख लेकर कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत और आकर्षक बनाना होगा। मेट्रो, बस और लोकल ट्रेनों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई-रिक्शा और साइकिल ट्रैक को बढ़ावा देकर निजी वाहनों की संख्या को कम किया जा सकता है। पार्किंग नीति को सख्ती से लागू करना होगा। मल्टी-लेवल पार्किंग और अंडरग्राउंड पार्किंग को अनिवार्य बनाना होगा। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के तहत डिजिटल भुगतान और स्लॉट बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाया जा सके।
इसके अलावा, कंजेशन चार्ज और कारपूलिंग को बढ़ावा देना होगा। सिंगापुर और लंदन की तर्ज पर कंजेशन चार्ज लगाने से ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सकता है। वाहनों की वहन क्षमता (Carrying Capacity) का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जरूरत से ज्यादा वाहनों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। वैकल्पिक परिवहन और नीति सुधार भी जरूरी हैं। साइकिल, पैदल चलने और ई-स्कूटर्स को बढ़ावा देने के लिए समर्पित लेन बनानी चाहिए। कामकाजी घंटों को विभाजित कर पिक-ऑवर के दबाव को कम किया जा सकता है।
समस्या के समाधान के लिए केवल बुनियादी ढांचे में बदलाव ही काफी नहीं है, बल्कि नागरिकों की सोच और आदतों में भी बदलाव लाना होगा। सार्वजनिक परिवहन को न केवल सुलभ, बल्कि सुविधाजनक और किफायती बनाना होगा, ताकि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम करें। सरकार को ठोस नीति बनाकर उसे प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना होगा, तभी भारतीय शहरों को ट्रैफिक और पार्किंग के जंजाल से मुक्त किया जा सकेगा। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले वर्षों में यह स्थिति और भयावह हो सकती है।