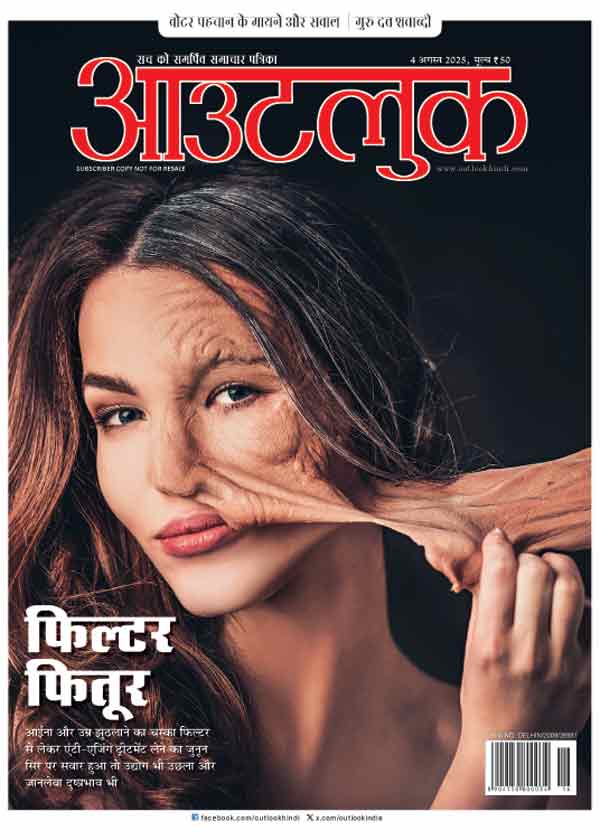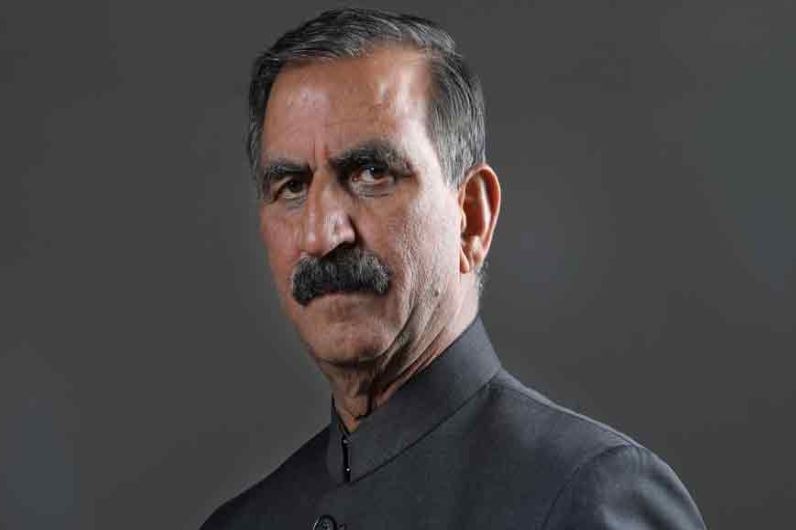केंद्र सरकार की 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) में जाति से संबंधित विस्तृत डेटा जुटाया गया था, लेकिन उसके नतीजों को सार्वजनिक नहीं किया गया। इससे अटकलों और विवादों को बढ़ावा मिला। इस बीच, कई राज्यों ने जाति गणना के लिए कदम उठाए। कर्नाटक में 2015 में जाति सर्वेक्षण किया गया और नए सिरे से इसे फिर करने का ऐलान किया गया। तेलंगाना ने भी हाल ही में यही किया गया। उत्तर प्रदेश में भी पहले ऐसे सर्वेक्षण की कोशिश हुई थी, पर सरकार बदलने से यह काम नहीं हो पाया। बिहार ऐसा राज्य हैं, जहां जाति गणना पूरी की गई, और इसी कारण देशव्यापी जाति जनगणना की मांग फिर उठ खड़ी हुई।
राज्यों की इस कोशिश में बेशक राजनैतिक गुणा-भाग था और उस पर अमल भी अलग-अलग तरीके से हुआ। लेकिन इन सबने मौजूदा देशव्यापी जाति जनगणना को आधार बनाया, जो काफी हद तक विपक्षी दलों के दबाव से तैयार हुआ है। शुरुआत में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के विचार को खारिज कर दिया था। हालांकि, इसके पीछे चुनावी और आरक्षण की राजनीति का जटिल जाल छिपा है।
ओबीसी की जटिलता
संविधान के तहत अधिसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के उलट ओबीसी श्रेणी की जातियां परिभाषित नहीं हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास केंद्रीय ओबीसी सूची (2,600 से अधिक समुदाय) है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाता है। हालांकि, राज्य सूचियां अलग हैं। कई राज्यों में कई और जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने अब दोनों में से किसी भी सूची के इस्तेमाल से बचने का विकल्प चुना है, जिससे ओबीसी श्रेणी को फिलहाल अपरिभाषित छोड़ दिया गया है।
आगे क्या होगा
जनगणना में जातियों और उप-जातियों को तो दर्ज किया जाएगा (ओबीसी श्रेणी को नहीं), लेकिन संभावना है कि राज्य इस डेटा का इस्तेमाल अपनी ओबीसी सूचियों को संशोधित करने या विस्तार करने के लिए करेंगे। इससे कई अहम प्रश्न उठने वाले हैं। मसलन,
. कच्चे आंकड़ों की व्याख्या कैसे की जाएगी
. क्या पुनर्वर्गीकरण या आरक्षण की नई मांगें उठेंगी
. सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में ओबीसी के दावे पर क्या असर होगा
. जनसंख्या में बदलाव से विभिन्न राज्यों में क्या अलग आवाज उठ सकती है
. उसके राजनैतिक निहितार्थ क्या होंगे
यकीनन, जाति गणना का फैसला केंद्र के राजनैतिक गुणा-भाग में बदलाव को दिखाता है, जो मुख्य रूप से विपक्ष की मांग है। इससे ये सवाल भी उठते हैं कि जाति संख्या आरक्षण के दायरे में बदलाव से लेकर सत्ता में साझेदारी की मांग तक भविष्य की नीतियों को कैसे प्रभावित कर सकती है? क्या ओबीसी श्रेणी के भीतर अधिक संख्या बल वाली प्रमुख जातियों में मजबूत पैठ वाली पार्टियों की छोटी जातियों, या जातियों के समूहों से टकराव की स्थिति बनेगी?
परिसीमन की समस्या
जनगणना में डेटा संग्रह 2026-2027 में किया जाना है, इसलिए पिछले अनुभव (2011 की जनगणना के डेटा 2013 में जारी किए गए थे) के आधार पर 2029 से पहले आंकड़े प्रकाशित होने की संभावना नहीं है। इसी गणना के आधार पर संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण) होना है, लेकिन सरकार परिसीमन में इस डेटा का उपयोग करेगी या नहीं, इस पर अभी अटकलें बनी हुई हैं, क्योंकि 2029 में ही आम चुनाव होना है।
निजी क्षेत्र में आरक्षण
राजनैतिक दलों और सामाजिक समूहों की ओर से जाति-आधारित आरक्षण को निजी क्षेत्र में विस्तारित करने की मांग बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य समग्र रोजगार में हाशिए पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। केंद्र सरकार की नौकरियां देश में कुल कार्यबल का 1.5-2 प्रतिशत से अधिक नहीं है। राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियों को जोड़ लें तो कुल सरकारी रोजगार का हिस्सा 15 प्रतिशत से कम है। इसलिए कई मुद्दे जाति गणना से ऐसे जुड़े हुए हैं, जो बेहद जटिल हैं।