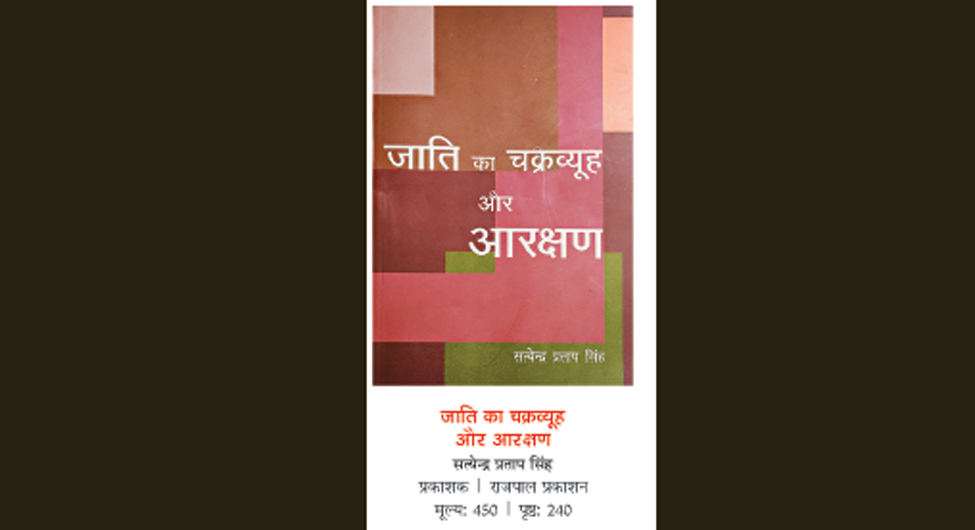सत्येन्द्र प्रताप सिंह की किताब ‘जाति का चक्रव्यूह और आरक्षण’ हमारे समाज में चली आ रही बहुत सारी धारणाओं और बनाए जा रहे बहुत सारे मिथकों का विश्वसनीय खंडन करती है। मसलन, अक्सर यह मिथक बनाया जाता है कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज का पुराना दुर्गुण नहीं है-पहले बस चार वर्ण थे जो सदियों बाद कई जातियों और उपजातियों में विभाजित हुए। मगर सत्येन्द्र प्रामाणिक संदर्भों के साथ बताते हैं कि जातियों का यह विभाजन भी अतिप्राचीन है। मनु ने 61 जातियों का उल्लेख किया है तो गुप्तोत्तर काल में इनकी संख्या सौ के पार चली जाती है।
दूसरी जिस महत्वपूर्ण बात की ओर यह किताब इशारा करती है, वह यह कि जाति-व्यवस्था जैसे-जैसे प्रारंभ और मजबूत हुई, वैसे-वैसे स्त्रियों की गुलामी बढ़ती गई। जाति-व्यवस्था पर आधारित समाज अपने नियमन में स्त्रियों और शूद्रों को एक जैसा दर्जा देता है। शूद्र जहां अस्पृश्य हैं, वहीं स्त्री महज भोग्या, जिसका कर्तव्य अपने स्वामी को हर तरह से खुश रखना है। इसके अलावा यह पूरी व्यवस्था ब्राह्मण के वर्चस्व पर टिकी हुई है। किताब बताती है कि “वराहमिहिर के मुताबिक ब्राह्मण का घर पांच कमरों का, क्षत्रिय का चार कमरों का, वैश्य का तीन और शूद्र का घर तीन कमरों का होना चाहिए।” जाति के मुताबिक कमरों के आकार भी तय होते थे।
मध्यकाल में इस जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक तीखा संघर्ष दिखाई पड़ता है। मझोली और निचली जातियों से आए संत कवि जाति को, धर्म को और ईश्वर तक को चुनौती देते हैं। कबीर के अलावा तुकाराम, रैदास, चोखामेला और हरिराम व्यास जैसे कवि हैं जिनके लेखन में इन सबकी सख्त आलोचना मिलती है। सत्येंद्र संत तुकाराम की एक कविता (अनुवाद में) का उल्लेख करते हैं जिसका जिक्र यहां समीचीन होगा- मेरे लिए ईश्वर मर गया है/उसे अन्य लोगों के लिए रहने दो/न तो उसकी कथा कहूंगा, न ही उसका नाम लूंगा/हम एक-दूसरे को मार कर जा चुके हैं/ उलाहना और प्रशंसा- बस यूं ही बीतते हैं मेरे दिन/ तुका कहते हैं, मैं खड़ा हूं शांत / बस ऐसे ही बीतता है मेरा जीवन।
लेकिन किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष के एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में आरक्षण के इस्तेमाल पर केंद्रित है। आरक्षण को लेकर भी हमारे सवर्ण समाज में कई भ्रांतियां मौजूद हैं। लोगों को बस यही खयाल आता है कि संविधान में दलितों और आदिवासियों के लिए कुछ ही बरस के आरक्षण का प्रावधान था, जिसे लगातार बढ़ाया जाता रहा है। इसके अलावा उनकी निगाह में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने की घोषणा की तारीख वह दिन है जब अपनी-अपनी जातियां भूल शहरों में एक होने की कोशिश कर रहा भारतीय समाज अचानक जातियों में विभाजित हो गया- एक दूसरे का कुलनाम पूछने लगा।
लेकिन सत्येंद्र प्रताप सिंह ब्योरे में जाकर बताते हैं कि किस तरह अंग्रेजों के समय ही आरक्षण की मांग और व्यवस्था दोनों शुरू हो गई थी। इसके अलावा इसके समानांतर ही इस आरक्षण को व्यर्थ बताने और बनाने के उपाय भी चल पड़े थे। दरअसल मामला सिर्फ जाति तोड़ने का नहीं है, अगड़े-पिछड़े की दरारें पाटने और अस्पृश्यता की लौह-दीवार गिराने का भी है। इस मोड़ पर आकर हम पाते हैं कि खुद को प्रगतिशील समझने और बताने वाले लोग भी इस दरार-दीवार को अगर उदारता से नहीं देखते तो भी इसकी यथास्थिति बनाए रखने के खामोश हामी हैं। किताब पढ़ते हुए यह एहसास नहीं जाता कि जाति प्रथा के विरुद्ध किसी निर्णायक लड़ाई में आरक्षण की भूमिका अपरिहार्य रहनी है। जाति तोड़ने के लिए अलग-अलग जातियों में बेटी और रोटी का रिश्ता जोड़ने की जरूरत बताने वाले डॉ. राम मनोहर लोहिया भी इस दरार को समझते थे और उन्होंने सामाजिक बराबरी के लिए ‘पिछड़ा पावे सौ में साठ’ का नारा दिया था। मगर जब मंडल ने इस मांग को कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध पूरी सवर्ण मानसिकता और बौद्धिकता खड्गहस्त हो गई। ’90 के दशक में मंडल को कमंडल में समोने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक अभियंत्रण शुरू किया, उसके कई चरणों की यह परिणति है कि आज पिछड़ों की बराबरी का एजेंडा हिंदू-बहुमतवाद के यथार्थ में तब्दील हो चुका है। इस दौरान आरक्षण के खिलाफ लड़ाई में कभी खुले मोर्चे बने तो कभी चुपचाप भितरघाती तरीकों की मदद ली गई।
किताब पर लौटें। सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने तल्लीनता और गंभीरता से उन सारे उपक्रमों पर नजर डाली है, जो अलग-अलग समय में अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण के संदर्भ में किए गए। कई कमेटियों की रिपोर्ट और उनकी सीमा किताब में बताई गई है।
इस क्रम में बिल्कुल ताजा समय तक आकर आर्थिक आधार पर आरक्षण के छल को भी लेखक ने पकड़ा और पहचाना है। वे बहुत सुचिंतित ढंग से यह लिखते हैं कि यह आर्थिक आरक्षण दरअसल आरक्षण की मूल अवधारणा को ही क्षतिग्रस्त करता है और पिछड़ों के लिए बचे-खुचे अवसरों में सेंधमारी करता है।
जाति-व्यवस्था को लेकर हमारे यहां बहुत सारा साहित्य है। वह हिंदी में भी आता रहा है। अांबेडकर की बेहद मशहूर ‘ऐनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ से लेकर गांधीवादी और समाजवादी विचारकों- लोहिया, किशन पटनायक और सच्चिदानंद सिन्हा तक का इस पर काम है। कुछ बरस पहले आई आनंद तेलतुंबडे की किताब को भी इसी क्रम में याद किया जा सकता है।
लेकिन सत्येन्द्र प्रताप सिंह की किताब जातिवाद की भीषणताओं, उसके विरुद्ध संघर्ष की जटिलताओं और आरक्षण की अपरिहार्यता से लेकर उसके साथ चल रहे घात-प्रतिघात को भी बहुत सहज ढंग से पकड़ती है। आम पाठकों के लिहाज से भी यह बहुत पठनीय किताब है जो काफी कुछ विचार करने लायक सामग्री सुलभ कराती है। किताब में ढेर सारे तथ्य, उनके संदर्भ और जरूरी आंकड़े हैं, जो इसे और समृद्ध और विश्वसनीय बनाते हैं।
जाति का चक्रव्यूह और आरक्षण
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
प्रकाशक | राजपाल प्रकाशन
मूल्य: 450 | पृष्ठ: 240