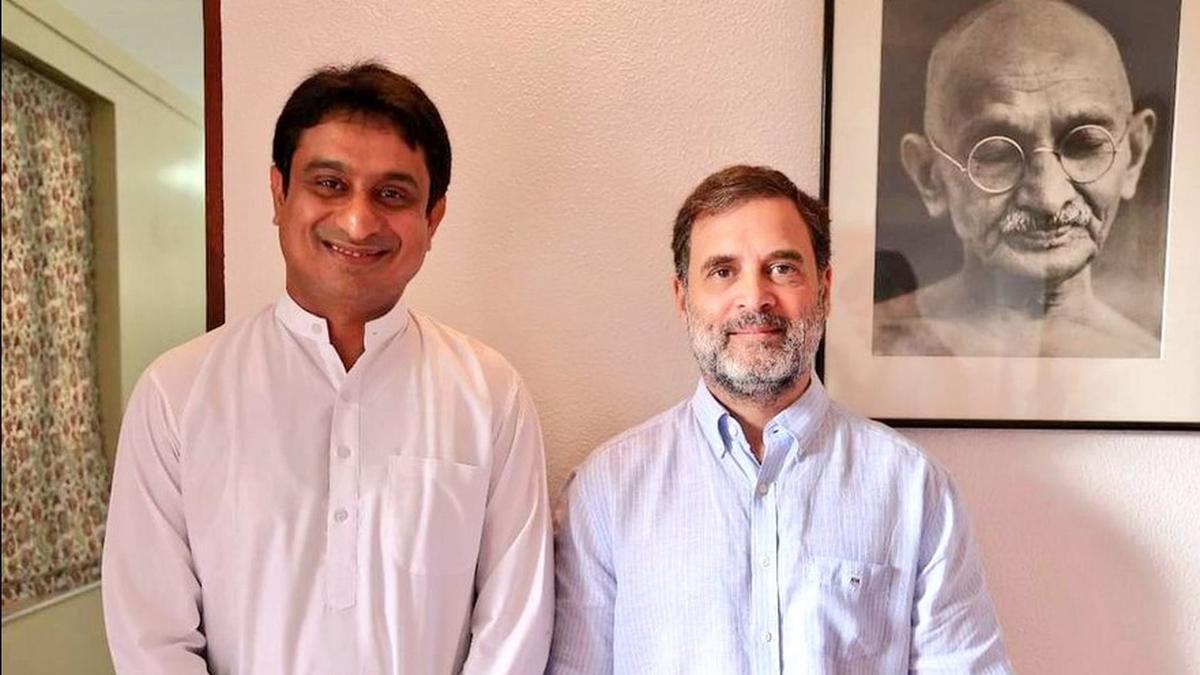भारतीय राजनीति में पिछले दस-बारह वर्षों में भारी परिवर्तन आया है। मनमोहन सिंह ने अपने वित्त मंत्रीत्व काल में जिस नयी आर्थिक नीति की शुरुआत किया था उसका चक्र उनके प्रधानमंत्रित्व काल में लगभग खत्म हो गया। इन वर्षों में राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत दार्शनिक सिद्वांतों में भारी बदलाव आया। स्वतंत्रता संग्राम से उपजे जिस दर्शन का एक रूप नेहरू का राजनैतिक चिंतन था, कांग्रेस पार्टी और मनमोहन-सोनिया नेतृत्व ने उसे त्याग कर घोर पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई। भारत के विकास के मॉडल को जिसे समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता माना जाता था, बाजारवाद के मॉडल में बदल दिया गया। इस बदलाव ने भारत में राजनैतिक उथल-पुथल मचा दी। बाजार व्यवस्था के प्रभाव में एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जिसके हिस्से में विकास का ज्यादा लाभ आया। लेकिन बड़े पैमाने पर लोग हाशिये पर आ गए। बाजार ने लोककल्याणकारी राज्य के बने बनाये शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे को लगभग तोड़ डाला। लोगों की राजनैतिक बैचेनी ने कांग्रेस सिस्टम को ही उखाड़ फेंका। क्षेत्रीय दलों का बोलबाला हो गया और अब कांग्रेस की उन पर निर्भरता हो गई। पिछले दस वर्षों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में जिस तरह का नेतृत्व बना उसमें जनता की आकांक्षाओं को दिशा देने की क्षमता नहीं रही और फिर हिंदुत्व का समय आ गया।जिस हिंदुत्ववादी पार्टी की लोकसभा में कभी केवल दो सीटें थीं, उसका धीरे-धीरे महत्व बढऩे लगा। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सम्माननीय हो जाना भारतीय समाज में भारी परिवर्तन का परिणाम है। जिस असंतुष्ट जनता ने कभी क्षेत्रीय दलों पर विश्वास किया था, अब उसका झुकाव बदल रहा है। संभव है, भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में हार भी जाए, लेकिन भारतीय राजनीति में इस बदलाव के दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं।
इस आपाधापी में सबसे बुरा हाल वामपंथी राजनीति का हो गया। उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है। इस देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। वामपंथी पार्टियां घोषित रूप से उनके लिए काम करती हैं। लेकिन पार्टी चुनाव में हाशिये पर पहुंच जाती है। यह एक पहेली है जिसे समझना मुश्किल है। हाशिये के लोगों की उनसे हुई नाउम्मीदी का नतीजा है बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी वामपंथी आंदोलन का राजनैतिक परिदृश्य में उभरना। उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में इन आंदोलनों के प्रति आम लोगों में सहानुभूति पैदा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण राजनैतिक विकल्प के रूप उनका उभरना सभव नहीं था क्योंकि भारतीय जनतंत्र को कुछ लोग भले ही छलावा मानें सच तो यह है कि इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं और जनतंत्र का विकल्प केवल और प्रभावकारी जनतंत्र ही है। वामपंथी आंदोलन को संगठनात्मक और रणनीति के स्तर पर भी जनतंत्र के महत्व को गंभीरता से लेना होगा। वामपंथी आंदोलन और कांग्रेस पार्टी ने जो जगह खाली की थी उसे भरने की होड़ भी लग गई। इसी बीच बड़े सुलझे तरीके से भ्रष्टाचार को मुद्दा बना कर देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया गया। अन्ना हजारे की गांधीवादी छवि ने लोगों को सड़क पर ला दिया, व्यवस्था में खोया हुआ विश्वास इस आंदोलन के लिए आधार बना। लेकिन आंदोलन शायद एक तरीका था एक नई पार्टी के बनाने का। फिर दिल्ली में सरकार बना कर आम आदमी पार्टी ने राजनीति में भूचाल ला दिया। अब हालत यह है कि कांग्रेस और वामपंथी राजनीति से निराश जनता ने 'आपÓ को एक ठोस आधार प्रदान किया है। संभव है आंदोलन की तरह मुख्य धारा में घुसने का यह एक तरीका मात्र हो। इस पार्टी की एक समस्या है कि इसके अपने लोगों ने डंके की चोट पर यह घोषणा कर दी है कि पार्टी के अंदर कोई जनतंत्र नहीं है। दिल्ली की सत्ता को नहीं संभाल पाने के कारण देश भर में लोगों ने इस पार्टी को लगभग बेकार मान लिया। दिल्ली के आने वाले चुनाव में इसका भविष्य फिर से तय होगा। यदि इसे अच्छी जीत मिली तो शायद एक राजनीतिक विकल्प के रूप में इसका विकास होगा या फिर पार्टी कई हिस्सों में बंट जा सकती है। खास कर जो समाजवादी राजनीति से लगभग बाहर हो गए थे और इस पार्टी से जुड़ कर अपने अस्तित्व की तलाश कर रहे थे उनके लिए फिर से नए रूप में सामने आने का एक मौका होगा।
इसी बीच सामजिक न्याय के पुरोधाओं को लगने लगा कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों में भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। नतीजतन मुलायम-नीतीश-लालू महागठबंधन बन गया। जनता परिवार का यह पुनर्मिलन कितना सफल होगा कहना कठिन है क्योंकि किसी ने फेसबुक पर ठीक ही कहा है कि ये सब फ्युज्ड बल्ब की तरह है। इनमें रोशनी की कोई खास उम्मीद नहीं है। सामाजिक न्याय की राजनीति अस्मिताओं के महिमामंडन पर टिकी थी। अस्मिता की राजनीति की एक सीमा होती है। उसके अंदर ही नई अस्मिताएं जन्म लेती हैं और पुराने को चुनौती देती हैं। दलित, महादलित के प्रयोग ने ऐसा ही कुछ किया है।
कुल मिला कर लगता है कि भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है जहां बहुत सी खाली जगहें हैं और उसके कई दावेदार भी हैं। अस्मिताओं का पुन: सम्मेलन होने वाला है। हाशिये के लोग इन प्रयोगों में अपना भाग्य आजमाएंगे। लेकिन उनके हाथ कुछ लगेगा नहीं। इसी बीच विश्व पूंजी का वर्चस्व भारतीय राजनीति पर बढ़ता जाएगा। समस्या यह है कि जनता के लिए यह सब कुछ कुछ समझना मुशिकल होगा क्योंकि पूंजी का प्रभाव उन्हें सीधा नहीं दिखेगा। पूंजी राजनीति पर पकड़ बनाये रखने के लिए मीडिया और संस्कृति का प्रयोग करेगी।
(लेखक जेएनयू में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं)
भारतीय राजनीति का बदलता चेहरा
भारतीय राजनीति में पिछले दस-बारह वर्षों में भारी परिवर्तन आया है। मनमोहन सिंह ने अपने वित्त मंत्रीत्व काल में जिस नयी आर्थिक नीति की शुरुआत किया था उसका चक्र उनके प्रधानमंत्रित्व काल में लगभग खत्म हो गया। इन वर्षों में राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत दार्शनिक सिद्वांतों में भारी बदलाव आया।

Advertisement
Advertisement
Advertisement