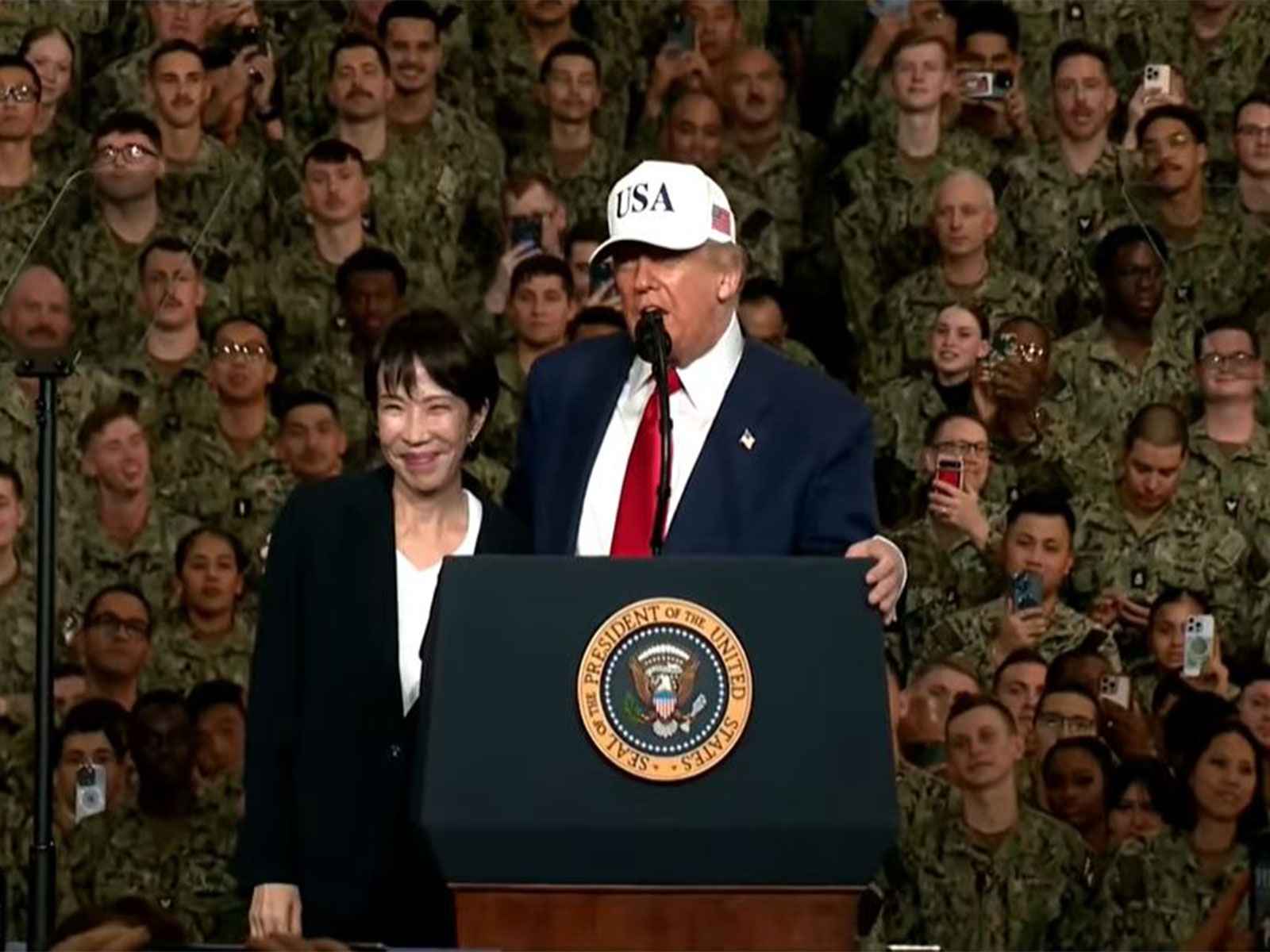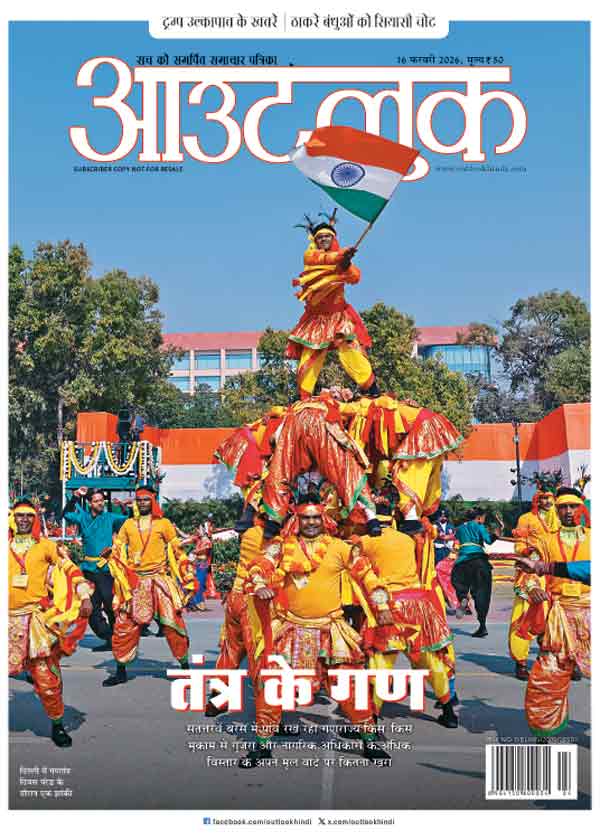- सचिन कुमार जैन
मंदसौर के पैंतालीस साल के लक्ष्मण सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने नौ पन्ने का आत्महत्या वक्तव्य छोड़ा था। जिसमें लिखा था कि उन पर दो साहूकारों का कर्ज था, जिसके बदले में वे 14.60 लाख रुपये चुकाने के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि परिजनों का कहना है कि उन पर बैंक, फायनेंस कंपनी और सोसाइटी का करीब 9.50 लाख रुपये का कर्जा था। जिसे वह नहीं चुका पा रहे थे।
दिक्कत यह भी है कि भारत के किसानों पर केवल बैंकों या वित्तीय संस्थाओं का ही कर्जा नहीं है। उन पर गैर-संस्थागत स्रोतों का भी भारी कर्जा है। इसके बारे में सरकार अधिकृत जानकारी नहीं देती है। नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन के सर्वेक्षण से जरूर यह अनुपात पता चलता है कि किसानों के कुल कर्जे में गैर-संस्थागत स्रोतों का कर्जा बहुत वजन रखता है। इस अनुपात के आधार पर आंकलन करने से पता चलता है कि भारत के किसानों पर कुल कर्जा 15.03 लाख करोड़ रुपये का था। इसमें से 6.25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था।
यदि 31 मार्च 2017 की स्थिति में नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) के ऋण अनुपात (कि किसानों पर कुल ऋण का 58.4 प्रतिशत संस्थागत ऋण है और 41.6 प्रतिशत ऋण गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया है) के आधार पर आंकलन करें तो किसानों पर 18.25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इसमें से संस्थागत ऋण 10.657 लाख करोड़ रुपये (अतारांकित प्रश्न 2897, कृषि एवं किसान मंत्रालय, दिनांक 11 अगस्त 2017, राज्यसभा) है। एनएसएसओ के मुताबिक किसानों पर 41.6 प्रतिशत गैर संस्थागत ऋण है। इस मान से उन पर 7.6 लाख करोड़ रुपये का ऐसा कर्ज है, जो आज की बहस से लगभग बाहर है।
चूंकि अभी सरकार ने राज्यवार संस्थागत ऋण से आंकड़े नहीं दिए हैं। अतः राज्यों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए हमने वर्ष 2015-16 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है।
अब यह बात स्पष्ट होने लगी है कि अकेले किसान कर्ज माफी से खेती का संकट मिटने वाला नहीं है। आज माफ कर देंगे और किसान को उसकी उपज की न्यायोचित-लाभदायी कीमत नहीं देंगे तो संकट वहीं का वहीं रहेगा। कुछ भी नहीं बदलेगा। कृषि ऋण के बारे में जब भी बात होती है, तब अक्सर संस्थागत ऋण (बैंकों-समितियों-सहकारी संस्थाओं से मिला ऋण) का ही सन्दर्भ दिया जाता है। जबकि भारतीय सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में गैर-संस्थागत ऋण (साहूकारों, पेशेवर कर्जदाताओं और स्थानीय व्यापारियों-आड़तियों के द्वारा दिया जाने वाला कर्ज) का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल रहा है। उसे जानबूझकर नजरंदाज किया जाता है। बहरहाल यह तो जरूरी है कि हम कृषि ऋण के चेहरे-मोहरे और उसके स्वरुप का आकलन करें। इस विश्लेषण में कृषि ऋण को तीन बिंदुओं पर केन्द्रित किया गया है। एक- संस्थागत कृषि ऋण की स्थिति, दो-गैर संस्थागत कृषि ऋण की स्थिति और तीन-सभी तरह के कृषि ऋण/समग्र ऋण की स्थिति।
(एक) संस्थागत कृषि ऋण
कृषि मूल्य और लागत आयोग की वर्ष 2017-18 की रबी और खरीफ की फसलों के लिए जारी रिपोर्ट के मुताबिक, “सरकार ने किसानों तक सस्ती ब्याज दर पर कृषि ऋण को पंहुचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सरकार लघु अवधि के लिए तीन लाख रुपये तक के ऋण सात प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है। इसमें प्रावधान यह है कि यदि किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, तो उन्हें चार प्रतिशत ही ब्याज देना पड़ता है। वर्ष 2004-05 में किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था, जो 2015-16 में बढ़कर 8.77 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। यह रिपोर्ट कहती है कि इस अवधि में फसल ऋण (यानि बीजों, उर्वरक, मजदूरी भुगतान, परिवहन समेत खेती के खर्चों के लिए) में आठ गुना की वृद्धि हुई है, यह 0.76 लाख करोड़ से बढ़कर 6.36 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीँ दूसरी ओर सावधि ऋण (खेती के लिए संसाधनों को मजबूत करने के मकसद से दिया जाने वाला ऋण) 0.49 लाख करोड़ से बढ़कर 2.05 लाख करोड़ ही रहा। इसका मतलब यह है कि किसान को अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही इतना कर्जा लेना पड़ रहा है कि वह खेती को बेहतर करने वाले कर्ज के बारे में नहीं सोच पा रहा है।
आत्महत्या और संस्थागत कृषि ऋण
आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में संस्थागत कृषि ऋण का वितरण समतामूलक नहीं है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों की कृषि ऋण तक पंहुच नहीं हुई है। पूर्वी राज्यों को देश के कुल संस्थागत कृषि ऋण का 10.6 प्रतिशत, मध्य क्षेत्र को 9.3 प्रतिशत और उत्तर पूर्वी राज्यों को केवल एक प्रतिशत ही मिला। बहरहाल किसानों की आत्महत्याओं और संस्थागत कृषि ऋण के संबंधों को समझना भी बहुत जरूरी है।
राज्यसभा में 31 मार्च 2017 को अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3357 के जवाब में कृषि मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2015-16 की स्थिति में किसानों पर लगभग आठ लाख करोड़ रुपये का संस्थागत ऋण था। इसमें से तमिलनाडु के किसानों पर 1.05 लाख करोड़ रुपये, कर्नाटक के किसानों पर 84.8 हजार करोड़ रुपये, पंजाब के किसानों पर 84.7 हजार करोड़ रुपये, आँध्रप्रदेश के किसानों पर 74.1 हजार करोड़ रुपये, राजस्थान के किसानों पर 67.6 हजार करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के किसानों पर 62.8 हजार करोड़ रुपये का ऋण था। देश में सबसे कम संस्थागत कृषि ऋण जम्मू और कश्मीर के किसानों पर (2.8 हजार करोड़ रुपये), झारखंड के किसानों पर (3.7 हजार करोड़ रुपये) और हिमाचल प्रदेश के किसानों पर (5.1 हजार करोड़ रुपये) था। बड़े राज्यों की सूची में उत्तरप्रदेश, जहां सबसे ज्यादा किसान हैं, पर 37.33 हजार करोड़ रुपये का संस्थागत कृषि ऋण था, जबकि बिहार के किसानों पर 40.5 हजार करोड़ रुपये बकाया थे। मध्यप्रदेश के किसानों पर 52.1 हजार करोड़ रुपये का कृषि ऋण दर्ज था।
कितने किसानों पर कितना ऋण?
नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन के रिपोर्ट क्र. 569 के मुताबिक भारत में 9.02 करोड़ किसान परिवार हैं। इनके सन्दर्भ में 7 फरवरी 2017 को लोकसभा में कृषि मंत्रालय ने बताया कि 4.69 करोड़ किसान (52 प्रतिशत) कर्जदार हैं। पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में 31.4 प्रतिशत ग्रामीण और 22.4 प्रतिशत शहरी परिवार कर्जदार हैं, किन्तु किसानों में यह कर्ज की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत है।
अभी हम केवल संस्थागत ऋण की बात कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में 4.69 करोड़ किसान परिवारों पर 8.78 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण है, यानि एक किसान परिवार पर 187313 रुपये का कर्ज है। देश के अलग अलग राज्यों में किसान की आर्थिक गुलामी का यह चित्र अलग अलग है। पंजाब में एक परिवार पर 11.29 लाख रुपये का कर्ज है, हरियाणा में 7.50 लाख रुपये, तमिलनाडु में 3.93 लाख रुपये, केरल में 3.98 लाख रुपये और मध्यप्रदेष में 1.90 लाख रुपये का कर्ज है। जिन राज्यों में सबसे कम कर्ज है, वे हैं - उत्तरप्रदेश (47.20 हजार रुपये), झारखण्ड (56.70 हजार रुपये), ओड़िशा (70.70 हजार रुपये)।
यदि सभी किसान परिवारों (9.02 करोड़) के मान से कुल संस्थागत ऋण (8.8 लाख करोड़ रुपये) का अनुपात निकाला जाता है तो स्पष्ट होता है कि भारत में एक किसान परिवार औसतन 97560 रुपये का कर्जदार है।
दोषपूर्ण नीतियों का परिणाम
यह एक दुधारी तलवार जैसी नीति है। एक तरफ तो यह किसान को कर्जदार बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को कम समर्थन मूल्य और खुले बाजार को ताकत देकर किसानों को ऐसी स्थिति में पंहुचाती है, जहाँ वे ब्याज तो छोड़िये, मूलधन भी चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। वर्ष 1996 से 2015 के बीच देश में 314718 किसानों आत्महत्या की है और इनमें से लगभग हर प्रकरण किसी न किसी रूप में कृषि कर्जे और किसान के जीवन में खत्म होते विकल्पों से जुड़ता रहा है। सरकार यह बात समझना ही नहीं चाहती है कि कर्ज चुकाने के लिए किसान की उपयुक्त और सम्मानजनक आय सुनिश्चित करना भी जरूरी है। भारत में सरकार ने कृषि ऋण देने की नीति बनायी, पर किसान की आय पर उसका रवैया पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार और किसान विरोधी रहा है। हमें इन परिस्थितियों में समझना होगा कि किसानों पर कर्ज लगातार बढ़ता गया है क्योंकि उन्हें अपनी उपज की लाभदायी कीमत नहीं मिल रही है और विपरीत परिस्थितियों में फसल का नुकसान होने पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई संरक्षण व्यवस्था नहीं है।
(दो) गैर संस्थागत ऋण
सामान्य तौर पर इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किसानों पर साहूकारों, आड़तियों, स्थानीय कर्ज देने वाले अन्य लोगों का कितना कर्ज बकाया है? सरकार के तंत्र में बैंकों, सहकारी समितियों या वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए कृषि ऋण की जानकारी जरूर मिल जाती है। दिसंबर 2016 में एनएसएसओ ने भारत में घरेलू ऋणग्रस्तता की स्थिति पर एक रिपोर्ट- क्र. 577 जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में किसानों पर जितना ऋण है, उसमें से 58.4 प्रतिशत संस्थागत ऋण है, जबकि 41.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत ऋण है। इसी आधार पर यदि हम यह मान लें कि वर्ष 2015-16 की स्थिति में 8.77 लाख करोड़ रुपये का वर्तमान ऋण (जिसकी जानकारी सरकार के पास है) संस्थागत ऋण है, तो इसे एसएसएसओ के अध्ययन के आधार पर 58.4 प्रतिशत माना जा सकता है। इस तरह हमें यह जानकारी मिलती है कि किसानों पर 6.25 लाख करोड़ रुपये का गैर संस्थागत (कुल कर्ज का 41.6 प्रतिशत) कर्ज भी है। जब हम किसानों के कर्ज के संकट, कर्ज माफी और कर्ज मुक्ति की बात करते हैं, तब इस राशि के बारे में भी स्पष्ट नीति और नजरिया होना जरूरी है जो फिलहाल तो नहीं है।
गैर संस्थागत ऋण के मामले में राजस्थान 1.30 लाख रुपये प्रति किसान और बिहार 1.02 लाख प्रति किसान सबसे आगे हैं। जबकि गैर संस्थागत ऋण की राशि आंध्रप्रदेश में 79.70 हजार रुपये, कर्नाटक में 78.30 हजार रुपये, पश्चिम बंगाल में 40.83 हजार रुपये और मध्यप्रदेष में 38 हजार रुपये है।
इसी अध्ययन से पता चलता है कि गैर-संस्थागत ऋण के मामले में पेशेवर साहूकार, कृषि सामग्री बेंचने वाले और स्थानीय दुकानदार सबसे अहम् भूमिका निभाते हैं। इस ऋण पर 30 प्रतिशत तक ब्याज दर होती है।
(तीन) सभी तरह के कृषि ऋण/समग्र ऋण
भारत में वर्ष 2015-16 की स्थिति में किसानों पर लगभग 15.03 लाख करोड़ रुपये का ऋण है। इसमें संस्थागत और गैर संस्थागत ऋण शामिल हैं। भारत में सभी 9.02 करोड़ किसानों पर प्रति किसान औसतन 1.67 लाख रुपये का ऋण है। इस मामले में पंजाब (8.4 लाख रुपये प्रति किसान), हरियाणा (5.46 लाख रुपये), तमिलनाडु (4.99 लाख रुपये), आँध्रप्रदेश (4.28 लाख रुपये) के किसान सबसे ज्यादा कर्जे में हैं।
जैसा कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने बताया है कि देश में 4.69 करोड़ किसान कर्जदार हैं। तब इस आधार पर प्रति कर्जदार किसान राशि 3.20 लाख रुपये निकल रही है। पंजाब में एक कर्जदार किसान पर 15.77 लाख रुपये, हरियाणा में 12.90 लाख रुपये, तमिलनाडु में 6.04 लाख रुपये केरल में 5.14 लाख रुपये, कर्नाटक में 4.98 लाख रुपये, राजस्थान में 4.92 लाख रुपये, आंध्रप्रदेश में 4.60 लाख रुपये, बिहार में 4.73 लाख रुपये, गुजरात में 3.60 लाख रुपये और मध्यप्रदेष में 3.29 लाख रुपये का आर्थिक भार और देनदारी है।
गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां यानी एनपीए और किसान- पिछले छः सालों से यह बहस जोरो पर है कि आर्थिक वृद्धि के नाम पर सरकार के पहलकदमी पर बैंकों ने उद्योगों-व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जमकर कर्जा दिया है। आर्थिक वृद्धि अक्सर हवा से भरे हुए गुब्बारे के रूप में बढ़ती हुई दिखाई देती है और जब उसमें कोई कांटा चुभता है, तो उसकी हवा निकल जाती है। सकल घरेलू उत्पाद का गुब्बारा भी ऐसे ही ऋण से फुलाया जाता रहा है। अब जब वह ऋण बैंकों के पास वापस नहीं आ रहा है, तो आर्थिक वृद्धि की हवा निकल रही है। हम व्यापक सवालों में नहीं जायेंगे। हम इस सन्दर्भ में बस किसानों का पक्ष समझने की कोशिश करेंगे। जिन्हें अनुत्पादक ऋण कहा जा रहा है, क्या वह मुख्य रूप से खेती और किसानों के कारण है? इस सवाल का जवाब है - नहीं!
31 मार्च 2017 की स्थिति में भारत के सरकारी और निजी बैकों के खाते में कुल 7.15 लाख करोड़ रुपये का ऐसा ऋण दर्ज था, जो वापस नहीं आ रहा है या चुकाया नहीं जा रहा है। इसमें से 6.41 लाख करोड़ रुपये सरकारी बैंकों के हैं।
यह जानना जरूरी है कि वास्तव में संकट से जूझ रहे कृषि क्षेत्र से जुड़े क्रियाकलापों के लिए दिए गए ऋण में से केवल 62.3 हजार करोड़ रुपये (कुल एनपीए का 8.7 प्रतिशत) ही गैर-निष्पादन परिसंपत्ति या न चुकाया गया ऋण है। इसके बावजूद किसानों का ऋण माफ करने की नीति को अर्थव्यवस्था के बर्बाद करने वाली नीति के रूप में प्रचारित किया जाता है। किसान बैकों का पैसा अनुचित तरीके से नही हथिया रहा है!
|
भारत में कुल कृषक परिवार और खेतिहर मजदूर परिवार |
|||
|
राज्य कुल |
कृषक परिवार (एनएसएसओ रिपोर्ट 569) |
कुल खेतिहर मजदूर (एनएसएसओ रिपोर्ट 577) |
कृषि पर आधारित कुल परिवार |
|
आंध्रप्रदेश |
3596800 |
1811900 |
5408700 |
|
बिहार |
7094300 |
3300000 |
10394300 |
|
छत्तीसगढ़ |
2560800 |
586100 |
3146900 |
|
गुजरात |
3930500 |
1111400 |
5041900 |
|
झारखंड |
2233600 |
58500 |
2292100 |
|
कर्नाटक |
4242100 |
1889900 |
6132000 |
|
केरल |
1404300 |
611700 |
2016000 |
|
मध्यप्रदेश |
5995000 |
1618000 |
7613000 |
|
महाराष्ट्र |
7097000 |
2929100 |
10026100 |
|
ओड़ीसा |
4493500 |
1107100 |
5600600 |
|
पंजाब |
1408300 |
345200 |
1753500 |
|
राजस्थान |
6483500 |
362900 |
6846400 |
|
तमिलनाडु |
3244300 |
2135500 |
5379800 |
|
तेलंगाना |
2538900 |
1137300 |
3676200 |
|
उतरप्रदेश |
18048600 |
2129400 |
20178000 |
|
प. बंगाल |
6362400 |
3230800 |
9593200 |
|
हरियाणा |
1569300 |
136500 |
1705800 |
|
जम्मू और कष्मीर |
128300 |
14700 |
143000 |
|
हिमाचल प्रदेश |
881100 |
10700 |
891800 |
|
भारत |
90201100 |
25039600 |
115240700 |
|
खेतिहर मजदूरों पर कर्ज |
||||||
|
राज्य |
प्रति 1000 परिवारों पर खेतिहर मजदूर परिवार संख्या |
प्रति 1000 खेतिहर मजदूर में से कर्जदार मजदूर |
औसतन नकद कर्ज रुपये में |
अनुमानित खेतिहर मजदूर संख्या |
कुल कर्ज राशि - करोड़ रू़ |
जनगणना 2011 के मुताबिक खेतिहर मजदूर दस लाख में |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
आंध्रप्रदेश |
209 |
494 |
31577 |
1811900 |
5721 |
16.97 |
|
बिहार |
235 |
339 |
15396 |
3300000 |
5081 |
18.35 |
|
छत्तीसगढ़ |
156 |
139 |
2206 |
586100 |
129 |
5.09 |
|
गुजरात |
189 |
171 |
16800 |
1111400 |
1867 |
6.84 |
|
हरियाणा |
53 |
394 |
25465 |
136500 |
348 |
1.53 |
|
हि. प्रदेश |
8 |
132 |
10995 |
10700 |
12 |
0.18 |
|
कर्नाटक |
244 |
437 |
24774 |
1889900 |
4682 |
7.06 |
|
झारखंड |
16 |
36 |
559 |
58500 |
3 |
4.44 |
|
केरल |
119 |
509 |
41432 |
611700 |
2534 |
1.32 |
|
मध्यप्रदेश |
191 |
165 |
8773 |
1618000 |
1419 |
12.19 |
|
महाराष्ट्र |
234 |
171 |
9179 |
2929100 |
2689 |
13.49 |
|
ओड़िशा |
142 |
165 |
2867 |
1107100 |
317 |
6.74 |
|
पंजाब |
125 |
315 |
16443 |
345200 |
568 |
1.59 |
|
राजस्थान |
44 |
338 |
42046 |
362900 |
1526 |
4.94 |
|
तमिलनाडु |
228 |
368 |
23941 |
2135500 |
5113 |
9.61 |
|
उत्तरप्रदेश |
88 |
266 |
10962 |
2129400 |
2334 |
19.94 |
|
जम्मू-कश्मीर |
11 |
183 |
1099 |
14700 |
2 |
0.55 |
|
तेलंगाना |
213 |
460 |
30335 |
1137300 |
3450 |
0 |
|
प. बंगाल |
229 |
205 |
7424 |
3230800 |
2399 |
10.19 |
|
भारत |
160 |
289 |
16141 |
25039600 |
40416 |
144.33 |
|
स्रोत - कालम 2 से 5 एसएसएसओ रिपोर्ट क्रमांक 577 (दिसंबर 2016 में जारी) - भारत में घरेलू ऋणग्रस्तता |
||||||
|
कालम 6 - एनएसएसओ द्वारा दिए गए आंकड़ों (कालम 3 और कालम 4) गणना |
||||||
|
कालम 7 - 18 नवंबर 2016 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 326 के उत्तर में दी गयी जानकारी |
||||||